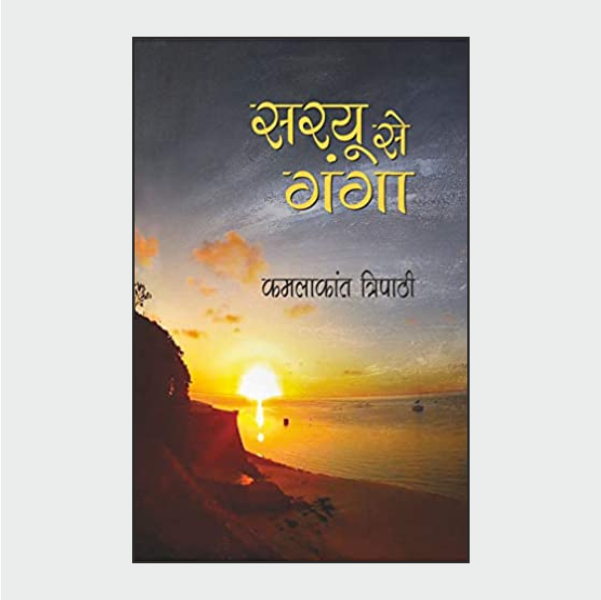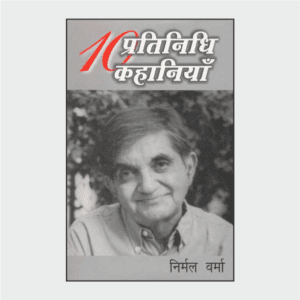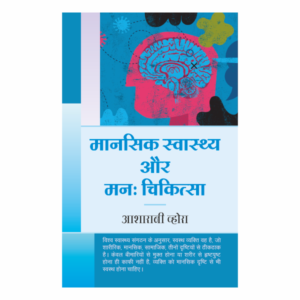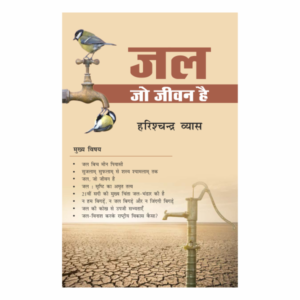अठारहवीं शती का उत्तरार्द्ध ऐसा कालखंड है जिसमें देश की सत्ता-संरचना में ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरोत्तर हस्तक्षेप एक जटिल, बहुआयामी राजनीतिक-सांस्कृतिक संक्रमण को जन्म देता है। उसकी व्याप्ति की धमक हमें आज तक सुनाई पड़ती है। सरयू से गंगा उस कालखंड के अंतहँढ्ों का एक बेलौस आईना है। सामान्य जनजीवन की अमूर्त हलचलों और ऐतिहासिक घटित के बीच की आवाजाही इसे प्रचलित विधाओं की परिधि का अतिक्रमण कर एक विशिष्ट विधा की रचना बनाती है। अकारण नहीं कि इसमें इतिहास स्वयं एक पात्र है और सामान्य एवं विशिष्ट, मूर्त एवं अमूर्त के ताने-बाने को जोड़ता बीच-बीच में स्वयं अपना पक्ष रखता है। इस दृष्टि से ‘सरयू से गंगा’ एक कथाकृति के रूप में उस कालखंड के इतिहास की सृजनात्मक पुनर्रचना का उपक्रम भी है।
‘सरयू से गंगा’ का कथात्मक उपजीव्य ध्वंस और निर्माण का वह चक्र है जो परिवर्तनकामी मानव-चेतना का सहज, सामाजिक व्यापार है। कथाकृति के रूप में यह संप्रति प्रचलित बैचारिकी के कुहासे को भेदकर चेतना के सामाजिक उन्मेष को मानव-स्वभाव के अंतर्निहित में खोजती है और समय के दुरूह यथार्थ से टकराकर असंभव को संभव बनानेवाली एक महाकाव्यात्मक गाथा का सृजन करती है।
फॉर्मूलाबद्ध लेखन से इतर, जीवन जैसा है उसे उसी रूप में लेते हुए, उसके बीहड़् के बीच से अपनी प्रतनु पगडंडी बनानेवाले रचनाकार को स्वीकृति और प्रशस्ति से निरपेक्ष होना पड़ता है। लेकिन तभी वह अपने स्वायत्त औज़ारों से सत्य के नूतन आयामों के प्रस्फुटन को संभव बना पाता है। तभी वह वैचारिक यांत्रिकता के बासीपन से मुक्त होकर सही अर्थों में ‘सृजन’ कर पाता है। ‘सरयू से गंगा’ ऐसे ही मुक्त सृजन की ताज़गी से लबरेज़ हे। लेखीपति, मामा, सावित्री, पुरखिन अइया, मतई, नाई काका, शेखर चाचा, जमील, रज़्जाक़ और जहीर जैसे पात्र मनुष्य की जिस जैविक और भावात्मक निष्ठा को अर्ध्य देकर अजेय बनाते हैं, वह अपने नैरंतर्य में कालातीत है। मानवता के नए बिहान की नई किरण भी शायद वहीं कहीं से फूटे।