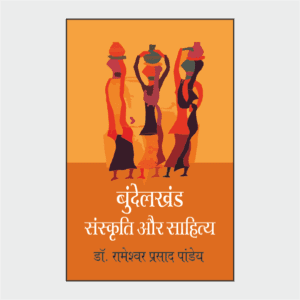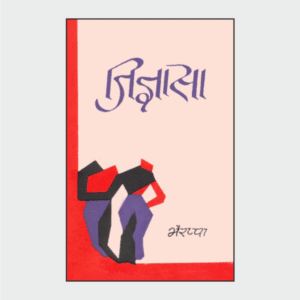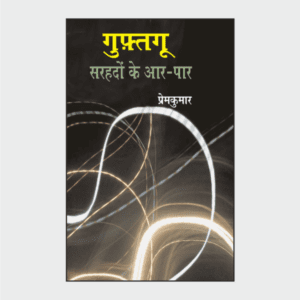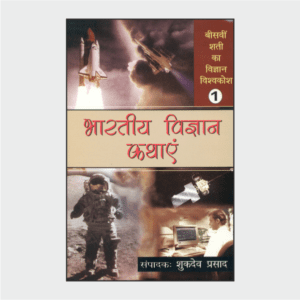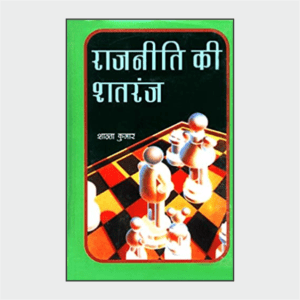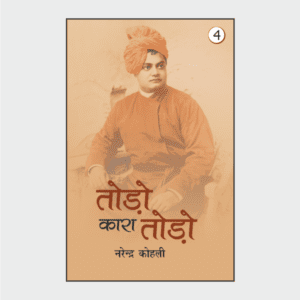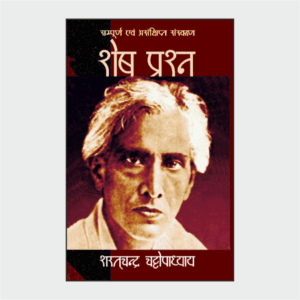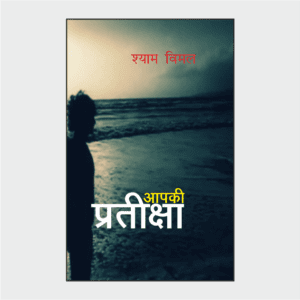Description
शेष अंत में’ सामाजिक पूष्ट्रभूमि पर आधारित एक यथार्थवादी पारिवारिक उपन्यास है । सन् ’42 के ‘भारत छोडों’ अन्दोलन से लेकर बीसवीं सदी के अंत तक के समय को शिद्दत के साथ पकड़ने और उसको जीवंत चित्रण की कोशिश इस उपन्यास में हम पाते हैं । बीजापुर गांव के एक संयुक्त परिवार की कथा के माध्यम से मध्यवर्गीय जीवन के सरोकारों, आदर्शों, विडंबनाओं और परिणतियों से हमारा साक्षात्कार होता है । समकालीन उपन्यास लिखने के दौर में जहाँ एक ओर निम्नवर्गीय जीवन और उसकी आकांक्षाओं पर खूब लिखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उच्चवर्गीय जीवन के मृत्युबोद्य, काल्पनिक चिंतन और वायवीय क्षणों पर । इसके विपरीत यह उपन्यास इस अर्थ में विशिष्ट है कि मध्यवर्गीय जीवन को उसकी संपूर्ण विशेषताओं एवं असंगतियों के साथ चित्रित करता है । उपन्यास को पढ़ते हुए संयुक्त परिवार की इस विलक्षणता से हम रू-ब-रू होते है, जहाँ घर में छोटे-छोटे सुख भी बड़े लगते हैं और बड़े दुख भी राई जितने छोटे । संयुक्त परिवार के विघटन के बाद नई परेशानियों और स्थितियों का विस्तार हम इस उपन्यास में पाते जहाँ सन् ’42 से 2000 तक के समय और संयुक्त परिवार से अकेले होते परिवार की त्रासदी प्रश्न बनकर उभरती है कि शताब्दी के अंत तक पहुंचते-पहुँचते हमने क्या पाया, क्या खोया ?
बीजापुर गांव के बब्बा जी के चार बेटों में संयुक्त परिवार के कपहैंधार बने गिरधर, उसके अन्य छोटे भाई मदन, श्याम और राधे के साथ गिरधर की पत्नी और भवहों (छोटे भाई की पत्नियां) के चरित्र विश्वसनीय रूप में उभरकर सामन जाते है, लेकिन सथा-नायक गिरधर और उसकी पत्नी के चरित्रांकन में अश्विनीकुमार दुबे को विशेष सफलता हाथ लगी हे। वे इस उपन्यास के यादगार चरित्र बन गए हैं । आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और समय की राजनीतिक उथल-पुथल को यह उपन्यास अधिक कारगर ढंग से प्रस्तुत करता है । विकास के नाम पर अंधी दौड़ में टूटते और मिटते भारतीय जीवन-मूल्य हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं ।
उपन्यास की रोचक पाठकीयता, घटनाओं की विश्वसनीयता और भाषा की रवानगी से निर्मित हुई है । भाषा की जीवंतता और सजगता उल्लेखनीय है । आंचलिक शब्दों के स्थानीय स्पर्श में गहराइयां हैं । लेखकीय संवेदना ने इसे एक यादगार उपन्यास बनाया है । -मिथिलेश्वर