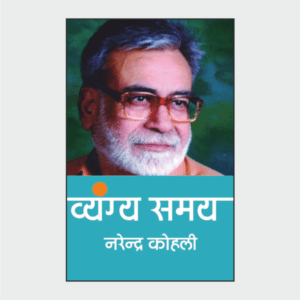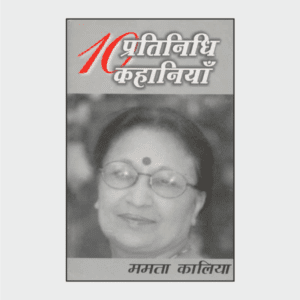व्यंग्य समय: नरेन्द्र कोहलीव्यंग्य समय: नरेन्द्र कोहली
देश के शुभचिंतक
“यह वाटिका हमारे मुहल्ले के लोगों के लिए है?” मैंने नगर निगम के अधिकारी से पूछा।
“जी हां!” वह बड़ी वक्रता से मुस्कराया, “वाटिका मेरे मुहल्ले वालों के लिए होती तो मेरे मुहल्ले में होती।”
“तो फिर ये फूल-पौधों के नाम और सैर करने वालों के लिए ये सारे निर्देश आपने अंग्रेजी में क्यों लगवा दिए हैं?” मैंने पूछा, “मेरे मुहल्ले वाले तो अपनी भाषा भी ढंग से लिख-पढ़ नहीं सकते। अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे?”
“ये निर्देश आपके मुहल्ले वालों के लिए नहीं हैं।” वे बोले।
“तो क्या ये निर्देश उन लोगों के लिए हैं, जो यहां कभी नहीं आएंगे?” मैंने पूछा, “क्योंकि आएंगे तो हमारे ही मुहल्ले वाले।”
वे हंसे, “यदि मैं आपको सच्चाई बता दूं तो आपको बुरा लगेगा।”
“नहीं! सच का क्या बुरा मानना।” मैं बोला, “आप बताएं तो!”
“आपके मुहल्ले वाले तो कोई निर्देश मानने से रहे।” वे बोले, “न वे घास पर चलने से रुकेंगे, न वे फूल न तोड़ने के आदेश का पालन करेंगे, न वे बाड़ को सुरक्षित रहने देंगे। तो फिर उनके लिए निर्देश लिखवाने का क्या लाभ?”
उनके उत्तर से मैं चमत्कृत हो गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे नगर निगम में इस उत्कृष्ट बुद्धि-मेधा के लोग भी हैं। एक भयंकर द्वंद्व मन में लिए मैं किकर्तव्यविमूढ़ खड़ा रह गया। निर्णय ही नहीं कर पाया कि अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उनका मुख, हाथ या माथा चूम लूं, उनके कंठ अथवा वक्ष से लग जाऊं; अथवा उनके चरणों पर लोट जाऊं। फिल्मी संस्कृति में चुंबन की प्रधानता है, लोक व्यवहार में आलिंगनबद्ध होने की और हमारी परंपरा में चरणों पर लोटना ही अधिक दिखाई देता है।
अपने अनिर्णय ने मुझे ‘कर्म’ के स्थान पर ‘शब्द’ का सहारा लेने को प्रेरित किया। बोला, “यह आपकी ही कूटनीतिक बुद्धि का प्रताप है कि आपने नगर निगम की कर्तव्यपरायणता को भी बचा लिया और हमारे मुहल्ले वालों के चरित्र को भी।”
इस बार चकित होने की बारी उनकी थी। बोले, “मैं कुछ समझा नहीं।”
“क्यों, इसमें ऐसा समझने को क्या है?” बोला, “आप ये निर्देश पट्ट न लगाते तो यह आरोप लगाया जाता कि नगर निगम वालों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया; और आप हिंदी में निर्देश लिखवा देते तो मेरे मुहल्ले वालों पर आरोप लगाया जाता कि वे नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करते। अब ऐसे में तो दोनों ही आरोपमुक्त हैं। आपने निर्देश लिखवा भी दिए, और उन्हें यह भाषा पढ़नी ही नहीं आती। ऐसे में वाटिका उजड़ भी जाए तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता।”
“व्यर्थ बात का बतंगड़ मत बनाओ। हमने उनके लिए तो निर्देश लिखवाए ही नहीं।” वे खीजकर बोले, “हमने तो अपने उन विदेशी मेहमानों के लिए, निर्देश अंग्रेजी में लिखवाए हैं, जो निकट भविष्य में यहां आने वाले हैं। अब सोचो तो, वे आएं और हिंदी में लिखे निर्देश न पढ़ पाएं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वे जान ही नहीं पाएंगे कि उन्हें यहां अपने कुत्तों को टहलना है या नहीं, घास पर जूते पहनकर चलना है या जूते उतारकर, फूल तोड़ने हैं या…”
“पर यहां कौन से विदेशी आने वाले हैं?” मैं बेहद डर गया था, जिस मुहल्ले में दो-चार विदेशी परिवार भी आ जाते थे, वहां मकानों का किराया दोगुना-तीन गुना हो जाता था। मैं अभी किराए पर था। वे विदेशी कुछ देर रुक नहीं सकते कि मैं भी अपना मकान बनवा लूं ताकि एक-आध खंड अच्छे किराए पर उन्हें दे सकूं।
“कौन आएगा, कहना मुश्किल है।” वे बोले, “जब देश के द्वार खोल ही दिए हैं तो कोई आए।”
मैं संभला, “यदि आपका संकेत विदेशी कंपनियों की ओर है तो मैं आपको बता दूं कि वे लोग हमारे मुहल्ले में रहने नहीं आएंगे।”
“यहां रहने के लिए तो अंग्रेज भी नहीं आए थे, पर सारा देश तो उनकी मुट्ठी में सिमट ही आया था।” वे बोले, “ अब आज हम हिंदी में निर्देश लिखवाएं, कल वे आकर अंग्रेजी में लिखवाएं। पैसा तो हमारे ही देश का खर्च होने वाला है। इसलिए हमने पहले ही निर्देश अंग्रेजी में लिखवा दिए हैं ताकि जब वे हमारा सारा देश खरीद लें तो न उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो; और न हमारे देश को दो-दो बार धन खर्च करना पड़े। कुछ आगे की भी सोच लेनी चाहिए।” उन्होंने रुककर मुझे देखा, “आखिर लांग-टर्म-प्लैनिंग किसे कहते हैं।… ”